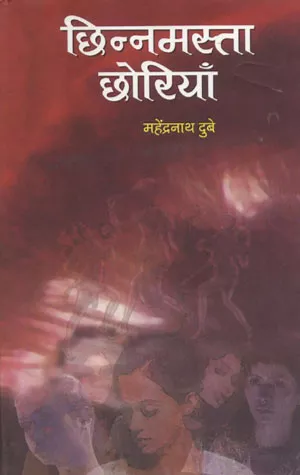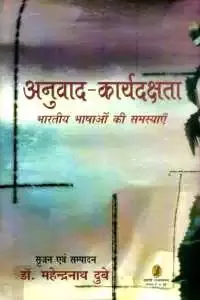|
सामाजिक >> छिन्नमस्ता छोरियाँ छिन्नमस्ता छोरियाँमहेन्द्रनाथ दुबे
|
167 पाठक हैं |
||||||
शरणार्थियों की समस्या पर आधारित उपन्यास
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करते मुसलमानों को भी फिर कभी वहाँ लौटने न
देने की पाकिस्तानी रणनीति, याहिया खान व भुट्टो और मुजीब की सोच,
शरणार्थियों की समस्या से जूझता भारतवर्ष, पाकिस्तानी की सेना के अत्याचार
के विरोध में जवान हिंदू लड़कियों का उठ खड़ा होना, कात्यायनी चक्रवर्ती
का साहसिक संग्राम, नागा बाबा के जीवन के भोगे हुए अनुभवों की
यथार्थ-भूमि, दोस्त-दुश्मन सभी की हित-चिंता में बराबर लगे रहने के कारण
नित्य जागरण में दैवी वरदान या अभिशाप ग्रस्तता के रहस्य की परतों को
छिन्न-भिन्न कर खोलता है उपन्यास-‘छिन्नमस्ता छोरियाँ’।
समर्पण
ढाका के छिन्नमस्ता देवी-मंदिर की तीन सीढ़ियों को-जहाँ से तीन अर्द्धमुखी
रक्तधाराओं में ऊपर की ओर छूटता दीखता है-खून का फौवारा-उसी अर्द्धचेतना
की प्रतिनिधि वर्तमान तीन विभूतियों-पूर्वस्थ छोर पर असमिया के वयोवृद्ध
किंतु चिर किशोर-प्रवीन-नवीन सभी साहित्यानुरागी जनता के हृदय-हार श्री
रेवती मोहन दत्त चौधुरी
-शीलभद्र उदीच्य छोर पर हिमालय के हिमालय से उन्नत भाल-हिमालय से दूर भी हिमालय के ही सहवास में रहनेवाले, साहित्य-रस में डूबे रहकर भी प्राचीन प्रभुमूर्तियों या पार्टी लाइन पर समीक्षा के नाम पर मठाधीश बने नवीन प्रभु-व्यक्तियों में से किसी के सामने भी माथा न झुकानेवाले सुहृदवर डॉ. देवेश ठाकुर
पश्चिमस्थ छोर की मायानगरी मुंबई के आयकर विभाग में आय की माया से चारों ओर घिरे रहकर भी-‘पुरइन पात रहत जल भीतर बूँद न ताको लागी’ के सचेत साधक भाई वीरेंद्र कुमार बरनवाल को सहज स्नेह संकोचवश।
-शीलभद्र उदीच्य छोर पर हिमालय के हिमालय से उन्नत भाल-हिमालय से दूर भी हिमालय के ही सहवास में रहनेवाले, साहित्य-रस में डूबे रहकर भी प्राचीन प्रभुमूर्तियों या पार्टी लाइन पर समीक्षा के नाम पर मठाधीश बने नवीन प्रभु-व्यक्तियों में से किसी के सामने भी माथा न झुकानेवाले सुहृदवर डॉ. देवेश ठाकुर
पश्चिमस्थ छोर की मायानगरी मुंबई के आयकर विभाग में आय की माया से चारों ओर घिरे रहकर भी-‘पुरइन पात रहत जल भीतर बूँद न ताको लागी’ के सचेत साधक भाई वीरेंद्र कुमार बरनवाल को सहज स्नेह संकोचवश।
छिन्नमस्ता छोरियाँ
पाकिस्तानी फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कौसर हुसैन पूर्वी
पाकिस्तान में नियुक्ति होकर जब जाते हैं तब तो मुक्तिवाहिनी के
स्वराज्य-आंदोलन को कुचलने का अभियान शुरू होता है, तो लगातार पाँच महीने
तक उन्हें एक पल को भी नींद नहीं आती। ढाका से कुछ दूर चाँदपुर के पास की
श्मशान काली मंदिर के अवधूत संत ओंकारानंद के चालीस वर्ष से न सोने की बात
सुन वे उनसे मिलने जाते हैं। हालाँकि पूर्वी बंगाल के ही मुसलमान उनके
सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि शेष सभी पाकिस्तानियों के दुश्मन बन चुके हैं।
ऐसी विरोधी दशा-देश-समझ सहज जिज्ञासावश इसका कारण पूछते हैं तो ऊँचे दर्जे
की पढ़ाई पढ़े हुए हूदा जैसे भाई उनकी नेक-नीयती तथा इंस्पेक्टर नश्कर
जैसे आदमी उनकी दिलेरी, पूर्वी पाकिस्तानी की बहू-बेटियों की इज्जत
बचानेवाला बताकर उनकी सुरक्षा में बने रहने का संकल्प बतलाते हैं।
श्मशान काली मंदिर से जो छिन्नमस्ता के मंदिर को डगर जाती है उस ओर बढ़ती एक पश्चिमी पाकिस्तानी वायु सैनिक अधिकारी की पत्नी स्वयं ही जब अपनी गला काट छिन्नमस्ता बनना चाहती है तब उसे रोकनेवालों के साथ वार्त्तालाप से स्पष्ट होता है कि जाति-धर्म से भी बड़ी चीज है-एक समाज में-एक साथ, एक भौगोलिक परिवेश में रहना। इसी से वह ठाने हुए हैं कि भारत के जिस फाजिल्का क्षेत्र की वह रहनेवाली है उसका पति उसके जीते-जी उस क्षेत्र पर बमबारी नहीं कर सकता।
पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करते मुसलमानों को भी फिर कभी वहाँ लौटने न देने की पाकिस्तानी रणनीति, याहिया खान, भुट्टो और मुजीब की सोच, शरणार्थियों की समस्या से जूझता भारतवर्ष, रूप-भारत सैनिक संधि, हिंदू सती-प्रथा की असलियत, सहायक सेवाइत (पुजारी) द्वारा दी गई जानकारियाँ, हिंदू जवान (युवा) लड़कियों को भारत पलायन न करने देकर जबरन रोक किसी पश्चिमी पाकिस्तानी की बीवी बनने को मजबूर करना। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में जवान हिंदू लड़कियों का उठ खड़ा होना। बारह जवान लड़कियों का कैद होना, कैद से उनका छूटना, कात्यायनी चक्रवर्ती का साहसिक संग्राम, नागा बाबा के जीवन के भोगे हुए अनुभवों की यथार्थ-भूमि जापानी राजनयिक की सहायता से छूटने का सरल मौका मिल जाने पर भी बँगलादेश छोड़कर भागने की बजाय वहीं बने रहकर संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ओंकारानंद को नींद न आने की बीमारी पर डॉ. मोर्त्ताजा का निदान, दोस्त-दुश्मन सभी की हित-चिंता में बराबर लगे रहने के कारण नित्य-जागरण के दैवी वरदान या अभिशाप-ग्रस्तता के रहस्य की परतों को छिन्न-भिन्न कर खोलता है उपन्यास-‘छिन्नमस्ता छोरियाँ’। इस औपनिषदिक आदेश के अनुपालनार्थ कि-‘त त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।’
-हे दूसरों के हितसाधक पालनहार ! उस ढकने को हटा दो, ताकि वे उस खरे सत्य को देख सकें। ढकना चाहे कितना भी बहुमूल्य हो, तोड़ फेंको उसे; उनके लिए जिनका सत्य ही धर्म है, जो सत्य की ही उपासना करते हैं।
श्मशान काली मंदिर से जो छिन्नमस्ता के मंदिर को डगर जाती है उस ओर बढ़ती एक पश्चिमी पाकिस्तानी वायु सैनिक अधिकारी की पत्नी स्वयं ही जब अपनी गला काट छिन्नमस्ता बनना चाहती है तब उसे रोकनेवालों के साथ वार्त्तालाप से स्पष्ट होता है कि जाति-धर्म से भी बड़ी चीज है-एक समाज में-एक साथ, एक भौगोलिक परिवेश में रहना। इसी से वह ठाने हुए हैं कि भारत के जिस फाजिल्का क्षेत्र की वह रहनेवाली है उसका पति उसके जीते-जी उस क्षेत्र पर बमबारी नहीं कर सकता।
पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करते मुसलमानों को भी फिर कभी वहाँ लौटने न देने की पाकिस्तानी रणनीति, याहिया खान, भुट्टो और मुजीब की सोच, शरणार्थियों की समस्या से जूझता भारतवर्ष, रूप-भारत सैनिक संधि, हिंदू सती-प्रथा की असलियत, सहायक सेवाइत (पुजारी) द्वारा दी गई जानकारियाँ, हिंदू जवान (युवा) लड़कियों को भारत पलायन न करने देकर जबरन रोक किसी पश्चिमी पाकिस्तानी की बीवी बनने को मजबूर करना। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में जवान हिंदू लड़कियों का उठ खड़ा होना। बारह जवान लड़कियों का कैद होना, कैद से उनका छूटना, कात्यायनी चक्रवर्ती का साहसिक संग्राम, नागा बाबा के जीवन के भोगे हुए अनुभवों की यथार्थ-भूमि जापानी राजनयिक की सहायता से छूटने का सरल मौका मिल जाने पर भी बँगलादेश छोड़कर भागने की बजाय वहीं बने रहकर संघर्ष करने की प्रतिज्ञा ओंकारानंद को नींद न आने की बीमारी पर डॉ. मोर्त्ताजा का निदान, दोस्त-दुश्मन सभी की हित-चिंता में बराबर लगे रहने के कारण नित्य-जागरण के दैवी वरदान या अभिशाप-ग्रस्तता के रहस्य की परतों को छिन्न-भिन्न कर खोलता है उपन्यास-‘छिन्नमस्ता छोरियाँ’। इस औपनिषदिक आदेश के अनुपालनार्थ कि-‘त त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।’
-हे दूसरों के हितसाधक पालनहार ! उस ढकने को हटा दो, ताकि वे उस खरे सत्य को देख सकें। ढकना चाहे कितना भी बहुमूल्य हो, तोड़ फेंको उसे; उनके लिए जिनका सत्य ही धर्म है, जो सत्य की ही उपासना करते हैं।
-महेंद्र
नाथ दुबे
1
कोयलिया बोले कहाँ-कहीं रात
‘‘झिरि-झिरि बरषाय
हाय कि गो भरसाय
आमार भाँगाँ घरे तोमा बिने।
सन-सन बहे हाओवा
मिछे गान गाओआ
मिछा जीवोन तोमा बिने।
‘‘झिरि-झिरि बरषाय
हाय कि गो भरसाय
आमार भाँगाँ घरे तोमा बिने।
सन-सन बहे हाओवा
मिछे गान गाओआ
मिछा जीवोन तोमा बिने।
सिंदूर बिखेरे आसमान जब आ फैला था आँखों में, दिन के चार बजे ही; तो आँखें
जुड़ा गईं। देखते-ही-देखते सिंदूरी रंग जो हलदी की पियराई ले पसरा तो ऐसा
लगा जैसा नौजवान लड़की की गेहुँआई गोराई की देह पर शादी की हलदी चढ़ा रही
हैं सखियाँ और बड़ी भौजाइयाँ। ठीक तभी आसमान की चादर जो झँवराई तो पूरी
उलटी कड़ाही की शक्ल का आसमान मयूर की गरदन के नीले रंग में ऐसा दमकने लगा
जैसे हिंदुओं के देवता श्रीकृष्ण की विश्वरूप देह। तभी से जो मन अनमना
हुआ, फिर तो उड़ा-उड़ा जा पहुँचा पश्चिमी पाकिस्तान के अपने शहर कराची के
इलाके में, जहाँ चार बजे के समय में ही आँखें चौंधिया देनेवाले सूरज की
देह जलाती किरणों और धूल-धक्कड़ से भरे आसमान के रू-बरू यहाँ के वातावरण
को रखने-परखने, पूर्वी पाकिस्तान की इस धरती और आसमान के छन-छन बदलते
चित्र-विचित्र रूप से जो तुलना कर-करके हर एक माने में इसे बेहतर ही पाता
रहा। दिन के साढ़े चार बजे ही शाम ढल जानेवाले इस देश में आठ बजे ही
गहराती गई इस रात में हाइवे (मुख्य सड़क) से उत्तर की ओर जाती सड़क पर
मोड़ लेते ही शुरू हुआ तो जंगल का इलाका, उसमें गुआ (सुपाड़ी) गाछों,
कटहल, डाभ (जंगली बड़े संतरे), केले हरसिंगार के पेड़-पौधों से घिरे घास
फूस की झोंपड़ियोंवाले दोनों ओर गाँवों के बीच से जो गुजरना हुआ तो
ड्राइवर को कार की हेडलाइट (सामने की बत्ती) और सारी बत्तियाँ बुझा देने
को कहने के साथ-साथ ही जो बारिश शुरू हुई तो अजीब नजारा यह पेश आया कि
बारिश की धारा का पानी इतना भक्क सफेद दिखा कि अँधियारी रात में भी बाहर
उजियारा-उजियारा सा आगे-आगे भागता लगा।
‘‘अँधेरे में भी उजियारा’-उड़ेल देती है इस देश की आबोहवा (जलवायु) तो मन की गहराई में मन मसोसे पड़ी उदासी को क्यों नहीं उखाड़ फेंक वहाँ भी जगा देती खुशी की लहर ? ताकि इस बरसाती रात में कुछ क्षण चैन आए, जीवन हो जाए निर्बंध, दवाएँ खाने से पा छुटकारा, होकर निर्द्वंद्व। सुख से मूँद सकूँ अपनी पलकें, ताकि तुम भी महसूस कर सको-‘बारिश से भीगती रात में जिंदगी के सुख की खुमारी।’-इतना भर ही सोच पाए थे पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के बुलंद लड़ाके शूरमा लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कौसर हुसैन साहब कि कानों में रस घोल गई बंगाली स्त्री-कंठ से निकलकर झिर-झिर...जीवोन तुम बिने।’ यहाँ रहते-रहते यहाँ की बँगला भाषा की जो थोड़ी सी समझ बन सकी है, उसी से मन में जो अर्थ उभरा, मन में टीस जगाने को वही काफी था। मगर कार की धीमी चाल पर भी जब गाँव के काफी पीछे छूटे जाने पर गाने के बोल सुनाई पड़ने बंद हो गए तब उन्होंने साथ में चल रहे बॉडी गार्डों (अंगरक्षकों) में से एक, जो बँगला भाषा के साथ-साथ उर्दू-फारसी के भी काफी अच्छे जानकार थे-मिर्जा जलाल हूदा नाम के, उनसे पूछ ही लिया-‘‘हूदा, इस गाने के क्या मायने हैं ? बरसाती देश की बरखा बुन्नी की बात है न, जो हमारी तरफ तो होती नहीं। इसीलिए वहाँ के मुसलमान नगमानिगारों (कवियों) के जेहन (मस्तिष्क) में तो ऐसी दर्द भीगी सोच कहनी आई ही नहीं।’’
‘‘हुजूर ! फिलहाल तो बारिश बहुत तेज हो गई है। थपेड़ों से बारिश के छींटे कार के शीशे की खिड़की पर पड़ रहे हैं। मगर अभी जब बारिश शुरू ही हुई थी, झिर-झिर झिरती झींसी की उसी रौ में वह विरहिणी बंगालिन गा रही थी कि इस लगातार हो रही रिमझिम बरसात में अभी तक तो जैसे-तैसे गुजर हुई। मगर आगे बचे रहने के लिए, सहारा देने को अब तो कोई ठोस उपाय बचा ही नहीं। जाने कब यह बारिश प्रचंड रूप ले ले और मारने लगे मूसलाधार थपेड़े। तब यह जो मेरी टूटी मड़ैया है, जिसे बस एक तुम्हारा ही सहारा हुआ करता था, थामे रखने का। तुम्हारे होने पर यह अपने टूटे-फूटे अंदाज में भी हमारी सुरक्षा कर लेती थी; परंतु अब जब कि तुम ही नहीं पास तो क्या भरोसा ! यह हमें बचाना तो दूर, खुद ही ढह-ढुहकर बरबाद न हो जाए ! ऊपर से बड़े जोरों की हवा कलेजा चीरती, सनसनाती सी बही जा रही है। ऐसे में बरसाती राग मल्हार में भी गाना गाऊँ तो भी सब वाहियात ही है। गीत गाना ही क्या ! सच पूछो तो तुम्हारे बिना जिंदगी जीना ही व्यर्थ है। वाहियात है, जिसके कोई मायने ही नहीं हैं। यहाँ तक कि जो होकर भी दरअसल कुछ है ही नहीं। सच होते हुए भी निरी झूठी है। जीवन सही में होकर भी वास्तव में झूठा है। दरअसल जीवन है ही नहीं यह।’’
‘‘वाह, क्या खूब ! तुम बंगाली मुसलामान क्या गजब की सोच लेते हो ! जबकि हमारे पश्चिमी मुसलामान तो ऐसा सोच ही नहीं सकते।’’ हुसैन साहब ने हुलसकर तारीफ की।
‘‘गुस्ताखी माफ कर सकें तो इस पर भी कुछ अर्ज करूँ, हुजूर !’’ हूदा नामक अंगरक्षक ने अदब के साथ पूछा।
हुँकारी भरे जाने पर फिर बोले पड़े, ‘‘सभी जगह एक से बढ़कर एक हुनरमंद हैं, हुजूर ! तवारीख (इतिहास) को अगर हम खालिस मजहबी नजरिए से केवल मुसलमानों में ही तलाशना चाहें तो उनकी भी कमी नहीं है और अगर भाषाई या जबानी नजरिए से देखें तब भी मुसलमानों में भी ऊँचे खयालों के लोगों की कमी कहीं नहीं रही है। हम बंगाली मुसलमानों को तो यह कभी खलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे तो हिंदू कवि चंडीदास, माइकेल, मधुसूदन दत्त, रवींद्रनाथ ठाकुर, जीवनानंद दास, बुद्धदेव बसु-सभी अपने बंगाली कवि हैं। जिस बँगलादेश को स्वतंत्र कराने की घोषणा बंगबंधु मुजीबुर्रहमान ने की है, उसका राष्ट्रगान-‘आमार सोना बाँगला आमी तोमाय भालोबासी।’ उसी रवींद्रनाथ की रचना को बनाया है। जो निखालिस हिंदू हैं और हैं खाँटी बंगाली। वर्षा-गानों यानी बरसाती-गानों में भी कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर सानी कोई नहीं। मगर हमें बताया गया है कि सारी आधुनिक भारतीय भाषाओं में बारिश का वर्णन करनेवाला सबसे बड़ा कवि तो आपका ही है-‘मलिक मुहम्मद जायसी’, जिसके ‘नागमती-विरह वर्णन’ के ‘बारहमासे’ का सानी काव्य-और तो और, अंगेजी में भी मुअस्सर (प्राप्त) नहीं।
‘‘जिस बँगला गान को सुनकर आपके दिल में अपने परम प्रिय की तड़प जगी ठीक उसी दर्दीली रागिनी की गूँज, बल्कि मैं तो कहूँ कि कहीं उससे भी अधिक सकारथ, कर्मठ, साथ-साथ रहने में ही परम प्रसन्न होते-चाहे लाखों कष्टों में ही जिंदगी क्यों न घिसट रही हो; ऐसी सहकर्मिता की, कोऑपरेशन की भावना की विशाल पटभूमि को तो मियाँ अब्दुर्रहीम खानखाना ने अपने छोटे से बरवै में ढाल दिया है-
‘‘अँधेरे में भी उजियारा’-उड़ेल देती है इस देश की आबोहवा (जलवायु) तो मन की गहराई में मन मसोसे पड़ी उदासी को क्यों नहीं उखाड़ फेंक वहाँ भी जगा देती खुशी की लहर ? ताकि इस बरसाती रात में कुछ क्षण चैन आए, जीवन हो जाए निर्बंध, दवाएँ खाने से पा छुटकारा, होकर निर्द्वंद्व। सुख से मूँद सकूँ अपनी पलकें, ताकि तुम भी महसूस कर सको-‘बारिश से भीगती रात में जिंदगी के सुख की खुमारी।’-इतना भर ही सोच पाए थे पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के बुलंद लड़ाके शूरमा लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कौसर हुसैन साहब कि कानों में रस घोल गई बंगाली स्त्री-कंठ से निकलकर झिर-झिर...जीवोन तुम बिने।’ यहाँ रहते-रहते यहाँ की बँगला भाषा की जो थोड़ी सी समझ बन सकी है, उसी से मन में जो अर्थ उभरा, मन में टीस जगाने को वही काफी था। मगर कार की धीमी चाल पर भी जब गाँव के काफी पीछे छूटे जाने पर गाने के बोल सुनाई पड़ने बंद हो गए तब उन्होंने साथ में चल रहे बॉडी गार्डों (अंगरक्षकों) में से एक, जो बँगला भाषा के साथ-साथ उर्दू-फारसी के भी काफी अच्छे जानकार थे-मिर्जा जलाल हूदा नाम के, उनसे पूछ ही लिया-‘‘हूदा, इस गाने के क्या मायने हैं ? बरसाती देश की बरखा बुन्नी की बात है न, जो हमारी तरफ तो होती नहीं। इसीलिए वहाँ के मुसलमान नगमानिगारों (कवियों) के जेहन (मस्तिष्क) में तो ऐसी दर्द भीगी सोच कहनी आई ही नहीं।’’
‘‘हुजूर ! फिलहाल तो बारिश बहुत तेज हो गई है। थपेड़ों से बारिश के छींटे कार के शीशे की खिड़की पर पड़ रहे हैं। मगर अभी जब बारिश शुरू ही हुई थी, झिर-झिर झिरती झींसी की उसी रौ में वह विरहिणी बंगालिन गा रही थी कि इस लगातार हो रही रिमझिम बरसात में अभी तक तो जैसे-तैसे गुजर हुई। मगर आगे बचे रहने के लिए, सहारा देने को अब तो कोई ठोस उपाय बचा ही नहीं। जाने कब यह बारिश प्रचंड रूप ले ले और मारने लगे मूसलाधार थपेड़े। तब यह जो मेरी टूटी मड़ैया है, जिसे बस एक तुम्हारा ही सहारा हुआ करता था, थामे रखने का। तुम्हारे होने पर यह अपने टूटे-फूटे अंदाज में भी हमारी सुरक्षा कर लेती थी; परंतु अब जब कि तुम ही नहीं पास तो क्या भरोसा ! यह हमें बचाना तो दूर, खुद ही ढह-ढुहकर बरबाद न हो जाए ! ऊपर से बड़े जोरों की हवा कलेजा चीरती, सनसनाती सी बही जा रही है। ऐसे में बरसाती राग मल्हार में भी गाना गाऊँ तो भी सब वाहियात ही है। गीत गाना ही क्या ! सच पूछो तो तुम्हारे बिना जिंदगी जीना ही व्यर्थ है। वाहियात है, जिसके कोई मायने ही नहीं हैं। यहाँ तक कि जो होकर भी दरअसल कुछ है ही नहीं। सच होते हुए भी निरी झूठी है। जीवन सही में होकर भी वास्तव में झूठा है। दरअसल जीवन है ही नहीं यह।’’
‘‘वाह, क्या खूब ! तुम बंगाली मुसलामान क्या गजब की सोच लेते हो ! जबकि हमारे पश्चिमी मुसलामान तो ऐसा सोच ही नहीं सकते।’’ हुसैन साहब ने हुलसकर तारीफ की।
‘‘गुस्ताखी माफ कर सकें तो इस पर भी कुछ अर्ज करूँ, हुजूर !’’ हूदा नामक अंगरक्षक ने अदब के साथ पूछा।
हुँकारी भरे जाने पर फिर बोले पड़े, ‘‘सभी जगह एक से बढ़कर एक हुनरमंद हैं, हुजूर ! तवारीख (इतिहास) को अगर हम खालिस मजहबी नजरिए से केवल मुसलमानों में ही तलाशना चाहें तो उनकी भी कमी नहीं है और अगर भाषाई या जबानी नजरिए से देखें तब भी मुसलमानों में भी ऊँचे खयालों के लोगों की कमी कहीं नहीं रही है। हम बंगाली मुसलमानों को तो यह कभी खलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे तो हिंदू कवि चंडीदास, माइकेल, मधुसूदन दत्त, रवींद्रनाथ ठाकुर, जीवनानंद दास, बुद्धदेव बसु-सभी अपने बंगाली कवि हैं। जिस बँगलादेश को स्वतंत्र कराने की घोषणा बंगबंधु मुजीबुर्रहमान ने की है, उसका राष्ट्रगान-‘आमार सोना बाँगला आमी तोमाय भालोबासी।’ उसी रवींद्रनाथ की रचना को बनाया है। जो निखालिस हिंदू हैं और हैं खाँटी बंगाली। वर्षा-गानों यानी बरसाती-गानों में भी कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर सानी कोई नहीं। मगर हमें बताया गया है कि सारी आधुनिक भारतीय भाषाओं में बारिश का वर्णन करनेवाला सबसे बड़ा कवि तो आपका ही है-‘मलिक मुहम्मद जायसी’, जिसके ‘नागमती-विरह वर्णन’ के ‘बारहमासे’ का सानी काव्य-और तो और, अंगेजी में भी मुअस्सर (प्राप्त) नहीं।
‘‘जिस बँगला गान को सुनकर आपके दिल में अपने परम प्रिय की तड़प जगी ठीक उसी दर्दीली रागिनी की गूँज, बल्कि मैं तो कहूँ कि कहीं उससे भी अधिक सकारथ, कर्मठ, साथ-साथ रहने में ही परम प्रसन्न होते-चाहे लाखों कष्टों में ही जिंदगी क्यों न घिसट रही हो; ऐसी सहकर्मिता की, कोऑपरेशन की भावना की विशाल पटभूमि को तो मियाँ अब्दुर्रहीम खानखाना ने अपने छोटे से बरवै में ढाल दिया है-
टूटि छानि, घर टुटिगा, खटियौ टूट।
पिय की साँसि उससवाँ सुख की लूट।।
पिय की साँसि उससवाँ सुख की लूट।।
‘‘वाह, क्या बात है ! क्या बात है ! प्रेमी की फेंकी
हुई साँस में जैसे खुशियों के फुहारे छूट रहे हैं, छुहारे लुटाए जा रहे
हैं। लूटते चलो, लूटते, चिंता किस बात की ?’’ हुसैन
साहब ने बच्चों की तरह ताली बजा-बजाकर शाबाशी दी। फिर बोले,
‘‘मगर चिंता की एक बात तो है न कि ये दोनों तो हिंदी
के कवि हैं।’’
‘‘इस बेसिर-पैर की चिंता को दूर करने को कुछ अर्ज करूँ, हुजूर ?’’
‘‘कहो-कहो, बारिश के छरक्कों से कम मजा मुझे तुम्हारी बातों में नहीं दीख रहा। ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे कभी नींद आ ही जाए।’’ हुसैन साहब हुलसकर बोले।
‘‘माफ करेंगे, हुजूर ! आपके देशवासी न अपने को मानते हैं, न अपनी को। इसी से तो भारतवर्षवाले बाजी मार लेते हैं।’’
‘‘क्या कहा ? क्या मकसद है तेरा ?’’ हुसैन साहब कड़के।
‘‘इसलिए तो कहता हूँ, हुजूर, कि हम सिपाही लोग आपसे बहुत-बहुत नीचे की श्रेणी के लोग हैं। हमें मुँह न लगाया करें। नहीं तो छोटे मुँह बड़ी बात निकल ही जाया करती हैं।
‘‘अरे, नहीं-नहीं ! माफ करो। माने, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुमने जो सोचा था, बेखौफ कहो।’’ हुसैन साहब ने ढाढ़स बँधाया।
‘‘हुजूर ! मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर आप अपने को, यानी मुसलमानों को ही अपना मानें तो ये दोनों ही शायर मुसलमान ही तो हैं। रहीम साहब तो खैर ऐसे खाँटी, फारसीदाँ ही नहीं खास फारस, अफगानिस्तान से आए, हिंदुस्तान के शाहंशाह हुमायूँ के जिगरी यार बैरम खाँ के शहजादे। ऐसे शहजादे, जिसने अपने बाप से अपना पैदाइशी हक कभी नहीं माँगा। नहीं तो जिस नन्हे से अकबर को हुमायूँ थार के रेगिस्तान में बैरम खाँ की गोद में फेंक भागे थे, अगर रहीम ने जिद की होती कोई और दूसरा बाप होता तो चौदह साल तक पालने-पोसने के बाद हिंदुस्तान को जीतकर अकबर को गद्दी पर न बिठाकर अपने बेटे रहीम को ही तख्त नवाजता। तब हिंदुस्तान की तवारीख (इतिहास) ही कुछ और होती, हुजूर ! और मलिक मुहम्मद जायसी तो उसके भी पहले की बादशाहत जौनपुरी के शेरशाह सूरी के गुरुओं में से थे।
‘‘अपने को न मानकर अगर अपनी, यानी कि अपनी भाषा को, माने कि हिंदी को, यानी कि उर्दू को ही मानते तो भी उनकी कविता आपकी होती। पूरे दक्षिण भारतवाले हिंदी को मुसलमानी जबान कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ हिंदू उर्दू को मुसलमानी जबान कहते हैं। मगर भाषा के जानकार जानते हैं कि जबानें हिंद की उर्दू जबान उर्दू-ए-मुअल्ला, यानी कि लाल किले के सबसे बड़े मुसलमानी फौजी तंबुओं की जमात की बोलचाल की भाषा ही हिंदी है। शुरू से आखिर तक, यानी कि अमीर खुसरो मलिक मुहम्मद जायसी, कबीरदास रहीम खानखाना, मीर तकी मीर मिर्जा गालिब मुहम्मद इकबाल, मजरूह सुलतानपुरी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी तक-तमाम मुसलमान फनकार अपने रिसाले बेखौफ इस जबान में रचते जा रहे हैं। हिंदू-मुसलिम की बात नजरअंदाज कर भारववर्षवाले उन्हें गले लगा अपना मान रहे हैं, उनकी जबान को अपनी मान रहे हैं। अंजाम सामने है कि-आज सारी दुनिया उन्हें सम्मान देने को मजबूर हुई जा रही है। जबकि एक आप लोग हैं कि इन अपनों को इस अपनी को पराया किए जा रहे हैं। दूसरी ओर वे हैं कि जिस बंगाली भाषा को हम अपनी मानते हैं, उसी के गीत को यानी रवींद्रनाथ ठाकुर के जन-गण-मन अधिनायक’ को उन्होंने अपना राष्ट्रगान बना लिया है, जबकि उसमें ज्यादातर हिंदी के पक्षपाती हैं। दूसरी ओर जिस उर्दू को हिंदी के ये पक्षपाती मुसलमानों की भाषा कहते हैं, उस उर्दू के ही नहीं बल्कि उर्दू के उस शायर के जिसे वे भारतवर्ष के बँटवारे की जड़ मानते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जिन्ना साहब तो पक्के राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हिंदू-मुसलिम एकता के पैरोकार पैगंबर थे, इसी से उस जमाने की भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने उन्हें ‘हिंदू-मुसलिम एकता का देवदूत’ कहा था; उस जिन्ना का दिमाग खा-खाकर उस अल्लामा इकबाल ने ही भारत के टुकड़े करवाए। पाकिस्तान नाम का अलग देश बनवा दिया। उस इकबाल के तराने ‘सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा’ को भी उन्होंने अपना राष्ट्रगान बना लिया है, जिस पर आज तक वहाँ कहीं से भी विरोध की कोई ‘चूँ’ की भी आवाज नहीं उठी।’’
‘‘आप तो इतने पढ़-लिखे हैं। बेकार में ही फौज में आ गए।’’ हुसैन साहब बोले, ‘‘आपको तो सब मालूम ही होगा, मगर यह ड्राइवर तौफीक आलम, ये दूसरे अंगरक्षक इसहाक हाशमी, इंस्पेक्टर मुश्ताक नश्कर तो उतना नहीं ही जानते होंगे। इस लिए मैं इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनवाने में मौलाना इकबाल की अहम भूमिका थी। भारतीय, जो उन्हें इतना आदर-सम्मान देते हैं, इसी से जाहिर कि वे भी इस बात को जानते-मानते हैं कि अल्लामा इकबाल की कोई खास भूमिका नहीं थी। अगर कहीं होती तो चूँकि बँटवारा होने के नौ साल पहले ही वे अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, सो इन नौ वर्षों में जिन्ना ही क्या, किसी के भी ऊपर से चढ़ा हुआ रंगीन मुलम्मा उतर जाता। सच्चाई तो यह है कि उतने बड़े भारतवर्ष की शासन-व्यवस्था में आ रही अड़चनों को देखकर सबसे पहले सन् 1883 में अंग्रेजी कूटनीजिज्ञ विल फ्रिड एस. ब्लांट ने ही सुझाव दिया था कि पूरे उत्तरी भारतवर्ष को मुसलमानों के शासन में और पूरे दक्षिणी भारत को हिंदुओं के शासन में देकर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाए और अंग्रेज तो बस दोनों से अपना लाभ आराम से उगाहते रहें। सन् 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों को जो लगातार एक पर एक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती आ रही थीं यहाँ के देशी राजाओं से, उनसे वे परेशान हो गए थे। सन् 1857 में मुसलमानों की अगुआई में जो हिंदू लड़े, तो अंग्रेजों के पैरों से जमीन खिसक गई। वह तो उनके खैरख्वाह सर सैयद अहमद खाँ ने सन् 1858 में उर्दू में एक किताब छपवाकर उसमें जो नुक्ता दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को जो अंग्रेजों ने एक ही रेजीमेंट में रखा, तो इसी में भूल हुई; क्योंकि इससे दोनों कौमों में एका बढ़ता चला गया। लिहाजा दोनों को अलग अलग बाँटकर रखना ही एकमात्र उपाय है।’’
‘घचाक्’ की एक जोरदार आवाज के साथ कार रुक गई तो अपनी बात के बीच ही हुसैन साहब पूछ बैठे, ‘‘क्यों ? कोई खतरा आ गया ?’’
‘‘नहीं हुजूर !’’ ड्राइवर तौफीक आलम बोला, ‘‘अब थोड़ी देर यहाँ रुकना ही होगा।’’
‘‘सो क्यों ? फिर यहाँ तो और भी ज्यादा अँधियारा है। बारिश का जोर कुछ कम हो जाने से तो और मजे से चल सकते हो।’’ वे इतना बोले ही थे कि कुछ चिहुँकते हुए फिर पूछ बैठे, ‘‘ये सामने काली दीवार-सी क्या चीज, बीच सड़क पर आ खड़ी हुई है ? मगर यह तो एक ओर को सरकती-सी जा रही है।’’
‘‘इस बेसिर-पैर की चिंता को दूर करने को कुछ अर्ज करूँ, हुजूर ?’’
‘‘कहो-कहो, बारिश के छरक्कों से कम मजा मुझे तुम्हारी बातों में नहीं दीख रहा। ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे कभी नींद आ ही जाए।’’ हुसैन साहब हुलसकर बोले।
‘‘माफ करेंगे, हुजूर ! आपके देशवासी न अपने को मानते हैं, न अपनी को। इसी से तो भारतवर्षवाले बाजी मार लेते हैं।’’
‘‘क्या कहा ? क्या मकसद है तेरा ?’’ हुसैन साहब कड़के।
‘‘इसलिए तो कहता हूँ, हुजूर, कि हम सिपाही लोग आपसे बहुत-बहुत नीचे की श्रेणी के लोग हैं। हमें मुँह न लगाया करें। नहीं तो छोटे मुँह बड़ी बात निकल ही जाया करती हैं।
‘‘अरे, नहीं-नहीं ! माफ करो। माने, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुमने जो सोचा था, बेखौफ कहो।’’ हुसैन साहब ने ढाढ़स बँधाया।
‘‘हुजूर ! मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर आप अपने को, यानी मुसलमानों को ही अपना मानें तो ये दोनों ही शायर मुसलमान ही तो हैं। रहीम साहब तो खैर ऐसे खाँटी, फारसीदाँ ही नहीं खास फारस, अफगानिस्तान से आए, हिंदुस्तान के शाहंशाह हुमायूँ के जिगरी यार बैरम खाँ के शहजादे। ऐसे शहजादे, जिसने अपने बाप से अपना पैदाइशी हक कभी नहीं माँगा। नहीं तो जिस नन्हे से अकबर को हुमायूँ थार के रेगिस्तान में बैरम खाँ की गोद में फेंक भागे थे, अगर रहीम ने जिद की होती कोई और दूसरा बाप होता तो चौदह साल तक पालने-पोसने के बाद हिंदुस्तान को जीतकर अकबर को गद्दी पर न बिठाकर अपने बेटे रहीम को ही तख्त नवाजता। तब हिंदुस्तान की तवारीख (इतिहास) ही कुछ और होती, हुजूर ! और मलिक मुहम्मद जायसी तो उसके भी पहले की बादशाहत जौनपुरी के शेरशाह सूरी के गुरुओं में से थे।
‘‘अपने को न मानकर अगर अपनी, यानी कि अपनी भाषा को, माने कि हिंदी को, यानी कि उर्दू को ही मानते तो भी उनकी कविता आपकी होती। पूरे दक्षिण भारतवाले हिंदी को मुसलमानी जबान कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ हिंदू उर्दू को मुसलमानी जबान कहते हैं। मगर भाषा के जानकार जानते हैं कि जबानें हिंद की उर्दू जबान उर्दू-ए-मुअल्ला, यानी कि लाल किले के सबसे बड़े मुसलमानी फौजी तंबुओं की जमात की बोलचाल की भाषा ही हिंदी है। शुरू से आखिर तक, यानी कि अमीर खुसरो मलिक मुहम्मद जायसी, कबीरदास रहीम खानखाना, मीर तकी मीर मिर्जा गालिब मुहम्मद इकबाल, मजरूह सुलतानपुरी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी तक-तमाम मुसलमान फनकार अपने रिसाले बेखौफ इस जबान में रचते जा रहे हैं। हिंदू-मुसलिम की बात नजरअंदाज कर भारववर्षवाले उन्हें गले लगा अपना मान रहे हैं, उनकी जबान को अपनी मान रहे हैं। अंजाम सामने है कि-आज सारी दुनिया उन्हें सम्मान देने को मजबूर हुई जा रही है। जबकि एक आप लोग हैं कि इन अपनों को इस अपनी को पराया किए जा रहे हैं। दूसरी ओर वे हैं कि जिस बंगाली भाषा को हम अपनी मानते हैं, उसी के गीत को यानी रवींद्रनाथ ठाकुर के जन-गण-मन अधिनायक’ को उन्होंने अपना राष्ट्रगान बना लिया है, जबकि उसमें ज्यादातर हिंदी के पक्षपाती हैं। दूसरी ओर जिस उर्दू को हिंदी के ये पक्षपाती मुसलमानों की भाषा कहते हैं, उस उर्दू के ही नहीं बल्कि उर्दू के उस शायर के जिसे वे भारतवर्ष के बँटवारे की जड़ मानते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जिन्ना साहब तो पक्के राष्ट्रवादी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हिंदू-मुसलिम एकता के पैरोकार पैगंबर थे, इसी से उस जमाने की भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने उन्हें ‘हिंदू-मुसलिम एकता का देवदूत’ कहा था; उस जिन्ना का दिमाग खा-खाकर उस अल्लामा इकबाल ने ही भारत के टुकड़े करवाए। पाकिस्तान नाम का अलग देश बनवा दिया। उस इकबाल के तराने ‘सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा’ को भी उन्होंने अपना राष्ट्रगान बना लिया है, जिस पर आज तक वहाँ कहीं से भी विरोध की कोई ‘चूँ’ की भी आवाज नहीं उठी।’’
‘‘आप तो इतने पढ़-लिखे हैं। बेकार में ही फौज में आ गए।’’ हुसैन साहब बोले, ‘‘आपको तो सब मालूम ही होगा, मगर यह ड्राइवर तौफीक आलम, ये दूसरे अंगरक्षक इसहाक हाशमी, इंस्पेक्टर मुश्ताक नश्कर तो उतना नहीं ही जानते होंगे। इस लिए मैं इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनवाने में मौलाना इकबाल की अहम भूमिका थी। भारतीय, जो उन्हें इतना आदर-सम्मान देते हैं, इसी से जाहिर कि वे भी इस बात को जानते-मानते हैं कि अल्लामा इकबाल की कोई खास भूमिका नहीं थी। अगर कहीं होती तो चूँकि बँटवारा होने के नौ साल पहले ही वे अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, सो इन नौ वर्षों में जिन्ना ही क्या, किसी के भी ऊपर से चढ़ा हुआ रंगीन मुलम्मा उतर जाता। सच्चाई तो यह है कि उतने बड़े भारतवर्ष की शासन-व्यवस्था में आ रही अड़चनों को देखकर सबसे पहले सन् 1883 में अंग्रेजी कूटनीजिज्ञ विल फ्रिड एस. ब्लांट ने ही सुझाव दिया था कि पूरे उत्तरी भारतवर्ष को मुसलमानों के शासन में और पूरे दक्षिणी भारत को हिंदुओं के शासन में देकर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाए और अंग्रेज तो बस दोनों से अपना लाभ आराम से उगाहते रहें। सन् 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों को जो लगातार एक पर एक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती आ रही थीं यहाँ के देशी राजाओं से, उनसे वे परेशान हो गए थे। सन् 1857 में मुसलमानों की अगुआई में जो हिंदू लड़े, तो अंग्रेजों के पैरों से जमीन खिसक गई। वह तो उनके खैरख्वाह सर सैयद अहमद खाँ ने सन् 1858 में उर्दू में एक किताब छपवाकर उसमें जो नुक्ता दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को जो अंग्रेजों ने एक ही रेजीमेंट में रखा, तो इसी में भूल हुई; क्योंकि इससे दोनों कौमों में एका बढ़ता चला गया। लिहाजा दोनों को अलग अलग बाँटकर रखना ही एकमात्र उपाय है।’’
‘घचाक्’ की एक जोरदार आवाज के साथ कार रुक गई तो अपनी बात के बीच ही हुसैन साहब पूछ बैठे, ‘‘क्यों ? कोई खतरा आ गया ?’’
‘‘नहीं हुजूर !’’ ड्राइवर तौफीक आलम बोला, ‘‘अब थोड़ी देर यहाँ रुकना ही होगा।’’
‘‘सो क्यों ? फिर यहाँ तो और भी ज्यादा अँधियारा है। बारिश का जोर कुछ कम हो जाने से तो और मजे से चल सकते हो।’’ वे इतना बोले ही थे कि कुछ चिहुँकते हुए फिर पूछ बैठे, ‘‘ये सामने काली दीवार-सी क्या चीज, बीच सड़क पर आ खड़ी हुई है ? मगर यह तो एक ओर को सरकती-सी जा रही है।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book